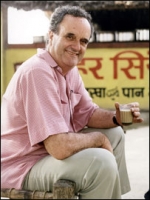‘गर्म हवा’ के अंतिम दृश्य में सलीम पाकिस्तान न जाने का फैसला कर रोजी रोटी की मांग को लेकर सड़क से गुजर रहे लाल झंडों से भरे एक जुलूस में शामिल हो जाता है. यह दृश्य दरअसल, सलीम का किरदार निभा रहे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के जीवन भर आम आदमी के बीच बने रहने की वास्तविकता को ही बयां करता है. बलराज अभिनेता होने के साथ ही एक लेखक और गंभीर संस्कृतिकर्मी थे. यह बलराज साहनी का जन्म-शताब्दी वर्ष है. इस मौके पर एक लेखक और अभिनेता के पीछे के बलराज साहनी और उनके संघर्ष की कहानी के कुछ हिस्से आपके लिए.
=============================================================
बलराज ने फिल्मों में कॅरियर बनाने का सपना तो पाल लिया था, लेकिन इस राह में कई चुनौतियां थीं. 1944 में मुंबई पहुंचने के बाद बलराज को पता चला कि वे चेतन आनंद की जिस फिल्म में काम करने के लिए आये थे, वह फिल्म आर्थिक मुश्किलों के कारण अधर में लटक गयी है. उन्होंने महसूस किया कि वे एक अनदेखी-अनजानी जगह पर अकेले हैं. सिनेमा के परदे पर अभिनेता बनने का ख्वाब एक और बात थी और फिल्म इंडस्ट्री में अपना पांव जमाना बिल्कुल दूसरी बात.
आर्थिक रूप से भी बलराज की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी. बीबीसी में काम करते हुए बचाये गये पैसे ही उनकी पूंजी थी. लेकिन यह पूंजी बहुत दिनों तक उनका साथ नहीं दे सकती थी. पिता से पैसा मंगाने को वे तैयार नहीं थे. चेतन ने बलराज की मुलाकात अपने कुछ जानने वालों से करायी. इसके बावजूद जो कुछ हो रहा था, उसका सामना उन्हें अकेले करना था. यह एक बेहद संघर्ष भरा दौर था.
सिनेमा में कॅरियर बनाने के उनके सपने की राह में कई रोड़े थे. सबसे बड़ा रोड़ा तो यही था कि उनकी उम्र 34 साल हो गयी थी. इस उम्र में वे यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि उन्हें सिनेमा के परदे पर युवा हीरो की भूमिका दी जाये. मुंबई में रहते हुए वे थके और मुरझाये नजर आने लगे थे. यह वह जमाना था जब भारतीय दर्शकों को हट्टे-कट्टे गोल चेहरे वाले हीरो पसंद आते थे.
आर्थिक मुश्किलें तो थी हीं. उनके लिए लिखी गयी सिफारिशी चिट्ठियां, वादे और भरोसे कुछ भी काम नहीं आ रहे थे. बलराज की स्थिति को भांपते हुए चेतन आनंद ने फनी मजूमदार से उनके लिए बात की और उन्हें अपनी किसी फिल्म में काम देने को कहा. फनी उस समय ‘जस्टिस’ फिल्म पर काम कर रहे थे. उन्होंने बलराज को इस फिल्म में मौका दिया. रिहर्सल का पहला दिन बलराज के लिए कई यादगार अनुभवों वाला रहा. उन्हें सिनेमा की दुनिया को पहली बार नजदीक से देखने का मौका मिला.
पहले दिन की रिहर्सल का जिक्र करते हुए बलराज ने लिखा है, ‘रिहर्सल के दौरान मुझे लगा कि मेरे जबड़े एंठ रहे हैं. मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूं लेकिन वे सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे. मेरी आवाज इतनी धीरे निकल रही थी कि उसे सुन पाना भी मुमकिन नहीं था. मुझे लगा कि फनी दा मेरे प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर करेंगे, लेकिन इसकी जगह उन्होंने प्रशंसा के भाव से मेरी तारीफ की- वेरी गुड शॉट ओके. यह सुनना था कि वहां तालियां बजने लगीं. लोग सीटी बजाने लगे. कुछ मेरे पास आये और मुझे बधाई देने लगे क्योंकि फिल्मों में यह मेरा पहला क्लोजअप था. फनी दा ने मेरे अकाउंट से रसगुल्ले मंगाये और सबमें बंटवाये.
हर कोई मेरी प्रशंसा कर रहा था. मैं आश्चर्यचकित था. मैं जान रहा था कि यह झूठी प्रशंसा है. लेकिन आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे थे? यह दरअसल, शोमैनशिप की दुनिया का बड़ा राज है, जिसे कोई आदमी धीरे-धीरे ही समझ सकता है. हां, यह झूठी प्रशंसा थी. स्टूडियो की दुनिया में कोई किसी से सच्चई बयां नहीं करता. यहां हर कोई सामने में आपकी तारीफ करता है और पीठ पीछे बुराई. बाहर के लोगों को यह छोटापन लग सकता है, लेकिन फिल्मी दुनिया के लोगों के लिए यह बड़ा बूस्टर है. यहां कोई मानसिक रूप से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता और एक झूठी दुनिया में रहता है. यहां कोई भी दूसरे के सपने के गुब्बारे में सुई नहीं चुभाना चाहता.
बलराज के लिए कैमरे का सामना करना मुश्किलों से भरा था. उनके पास स्टेज का अनुभव था. बीबीसी में अनाउंसर रहते हुए उन्होंने नॉर्मल स्पीच की कला भी सीखी थी, जो आने वाले समय में उनके बेहद काम आने वाली थी. कैमरे के सामने सहज होने में उन्हें काफी वक्त लगा. खुद बलराज साहनी के मुताबिक कैमरे के सामने जाना मुझे कुछ ऐसा लगता था मानों किसी राक्षस के सामने खड़ा कर दिया गया है. कई बार रिहर्सल में भी सब कुछ सामान्य रहता लेकिन कैमरा सामने आते ही पता नहीं अचानक क्या होता था कि मेरा एक-एक अंग अकड़ जाता था. मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती थी.
‘जस्टिस’ के बाद फनी दा के साथ बलराज ने उनकी अगली फिल्म ‘दूर चलें’ में भी काम किया. इस फिल्म में काम करते हुए बलराज साहनी इप्टा के संपर्क में आये. ‘दूर चलें’ के बाद आयी फिल्म ‘गुड़िया’. इस फिल्म के सेट पर आने से पहले बलराज इप्टा की प्रसिद्ध फिल्म ‘धरती के लाल’ में काम कर चुके थे. जिसे लिखा और निर्देशित किया था केए अब्बास ने. अपनी कई कमियों के बावजूद इस फिल्म ने एक नया ट्रेंड शुरू किया, जिसे विमल रॉय और सत्यजीत रॉय जैसे निर्देशकों ने आगे बढ़ाया. अब तक कैमरे के सामने उनका डर भी कम होने लगा था.
इप्टा के साथ बलराज साहनी का जुड़ाव बढ़ता जा रहा था और वे सिनेमा के साथ उसमें भी सक्रिय थे. लेकिन तब तक कम्युनिस्ट राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव आ गया था. पार्टी ने नेहरू के खिलाफ विरोध का रुख अपना लिया था. इस नयी नीति ने इप्टा के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित किया. उधर सरकार की नीतियां भी दमनकारी होने लगीं. इप्टा के कई पुराने सदस्य अलग हो गये. दूसरे कारणों से भी इप्टा के सदस्यों की संख्या कम होती गयी. ऐसे में इप्टा के प्रदर्शन काफी मुश्किल होते गये. उनके प्रदर्शनों पर पुलिस का पहरा होता था. लेकिन बलराज साहनी 1949 में अपनी गिरफ्तारी तक लगातार इप्टा से पूरी शिद्दत से जुड़े रहे. जेल से छूटने के बाद चेतन आनंद की फिल्म ‘बाजी’ की कहानी और स्क्रिप्ट लिखी. ‘हलचल’ फिल्म में काम किया.
‘हलचल’ के ठीक बाद बलराज को जिया सरहदी की फिल्म ‘हम लोग’ का प्रस्ताव मिला. इसमें उन्हें एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बेरोजगार युवक की भूमिका मिली. यह पहली फिल्म थी जिसमें बलराज काफी हद तक अपने रंग में नजर आये और कैमरे के सामने की उनकी अकड़न खत्म सी हो गयी. ‘हमलोग’ सफल रही और बलराज के अभिनय को काफी सराहा गया. अब वे आर्थिक रूप से भी बेहतर स्थिति में थे. ‘दो बीघा जमीन’ में उनकी प्रतिभा पूरी तरह परवान चढ़ पायी. वे अपने किरदार के साथ एकाकार हो गये और एक बेहतरीन स्क्रीन अभिनेता के तौर पर उनकी पहचान स्थापित हो गयी.
मुंबई के उपनगर जोगेश्वरी में दूधवालों की एक बस्ती है. ये दूधवाले उत्तर प्रदेश से हैं. जिस दिन बलराज को ‘दो बीघा जमीन’ के लिए चुना गया उस दिन से ही उन्होंने जोगेश्वरी के इन दूधवालों की कॉलनी में जाना शुरू कर दिया. वे गौर से दूधवालों के जीवन को देखा करते थे. उनके बातचीत करने, उठने-बैठने के तरीके पर गौर करते थे. उन्होंने लिखा है कि ‘दो बीघा जमीन’ में मेरी सफलता के पीछे इन दूधवालों की जिंदगी का नजदीकी मुआयना काफी काम आया.’ फिर कलकत्ता में शूटिंग के दौरान उनकी बिहार से आये एक रिक्शे वाले से मुलाकात हुई.
जब बलराज ने उसे फिल्म की कहानी सुनाई तो वह रोने लगा और उसने बताया कि यह तो बिल्कुल मेरी कहानी है. उसके पास भी दो बीघा जमीन थी, जो उसने एक जमींदार के पास गिरवी रखी थी और वह उसे छुड़ाने के लिए पिछले पंद्रह साल से कलकत्ता में रिक्शा चला रहा था. हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उस जमीन को कभी हासिल कर पायेगा. इस अनुभव ने उन्हें बदल कर रख दिया. उन्होंने खुद से कहा कि ‘मुझ पर दुनिया को एक गरीब, बेबस आदमी की कहानी बताने की जिम्मेदारी डाली गयी है, और मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के योग्य होऊं या न होऊं, मुझे अपनी ऊर्जा का एक एक कतरा इस जिम्मेदारी को निभाने में खर्च करना चाहिए.’
आनंद बाजार पत्रिका में एक फिल्म समीक्षक ने फिल्म में बलराज साहनी के प्रदर्शन पर टिप्पणी की थी, ‘बलराज साहनी के अभिनय में एक जीनियस की छाप है.’ यह जीनियस उस रिक्शेवाले की देन थी. सोवियत संघ के एक निर्माता ने कहा कि बलराज साहनी के चेहरे पर एक पूरी दुनिया दिखाई देती है. बलराज ने लिखा,‘यह दुनिया उस रिक्शेवाले की थी. शर्म की बात है कि आजादी के 25 साल बाद भी वह चेहरा नहीं बदला है.’
बलराज की सफलता का राज था कि वे किसी किरदार को निभाते वक्त उसमें अपना दिल ही नहीं, आत्मा भी झोंक देते थे. काबुलीवाला फिल्म करते वक्त उन्होंने पठान काबुलीवाला के जीवन को नजदीक से जानने के लिए उसका गहन अध्ययन किया. यही कारण है कि जब आप बलराज की किसी फिल्म को याद करते हैं, तो बलराज याद नहीं आते वह किरदार याद आता है. हर किरदार अपने आप में अलग नजर आता है. अभिनेता बलराज गायब हो जाता है. वह अपनी पहचान को किरदार में घुला देते थे. यह इस कारण होता था क्योंकि वे किरदार से गहरे स्तर पर जुड़ जाते थे. बलराज कहते थे कि एक्टिंग सिर्फ कला नहीं है, यह एक विज्ञान भी है.’
लेकिन इससे बढ़कर भी शायद एक चीज थी, वह था बलराज का सामाजिक सरोकार. वे किसी किरदार को उसके सामाजिक संदर्भो से जोड़ कर देखते थे. उन्होंने मार्क्सवाद के महत्व को स्वीकार किया. उनकी नजरों में मार्क्सवाद सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि दुनिया जैसी है, उसे उसी रूप से देखने की सीख देता है. वे मेहनती तो थे ही साथ ही हमेशा जमीन से जुड़े रहे. साधारण बने रहे. हमेशा दूसरों से सीखते रहते थे. लोगों की दिल खोल कर प्रशंसा कर सकते थे. घंटों तक सेट पर दिलीप कुमार को अभिनय करते देखते थे, उनके अभिनय से सीखने की कोशिश करते थे.
वे इतने साधारण बने रहे इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि वे स्क्रीन अभिनेता के समाज में महत्व को लेकर किसी भ्रम में नहीं पड़े न उसे पाला. एक बार मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में उनके साथ जैकेट खरीदने एक दुकान में गया. जैसा कि अकसर होता था, थोड़ी देर में लोगों ने उन्हें पहचान लिया और वहां भीड़ जमा होती गयी. वे काफी सहज भाव से लोगों को कागजों पर डायरियों पर यहां तक कि रुपये के नोटों पर ऑटोग्राफ देते रहे और बाहर निकलने की कोशिश करते रहे.
जब हम कार के पास पहुंचे तो मैंने कहा,‘यह कितना अद्भुत है. लोग आपको कितना चाहते हैं.’ बलराज ने कहा, ‘तुमने हमेशा लोगों को प्रशंसा करते सुना है. उनकी आलोचना नहीं सुनी है. जब एक एक्टर अपनी पीठ घुमाता है, तो लोग उसकी आलोचना भी करते हैं. किसी भ्रम में मत रहो. एक्टर को देखने के लिए जो भीड़ जमा होती है वह केवल एक सितारे के प्रति सामान्य जिज्ञासा के कारण जमा
होती है.’
( भीष्म साहनी द्वारा रचित बलराज साहनी की जीवनी ‘बलराज माय ब्रदर’ का अनुवादित अंश )
अनुवाद किया है अवनीश मिश्रा ने